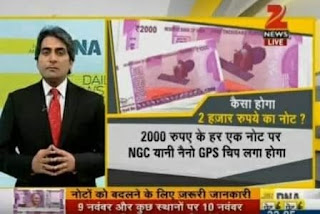||यह कोई विज्ञापन नहीं है||
पिछले एक दशक में हिंदी के गंभीर पाठकों के बीच बार-बार जो नाम उभरा है, वह है Ashok Kumar Pandey और Dakhal Prakashan Delhi का.साहित्यिक दलबंदी और बड़बोलेपन से दूर मगर हिंदी पुस्तक-संस्कृति के साथ पूरी आत्मीयता से समर्पित यह आन्दोलन कब हिंदी पाठकों की जरूरत बन गया, बता पाना मुश्किल है. एक कवि, कथाकार और अनुवादक के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके अशोक जिस एक किताब की वजह से एकाएक सतह पर उभर आए, वह थी उनकी बहुचर्तित किताब कश्मीरनामा.
सामाजिक इतिहास और संस्कृति को वस्तुनिष्ठ रूप में, अपने समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप लिखने का यह शऊर कदाचित पहली बार हिंदी में सामने आया है.
हिंदी समाज से जुड़ी बौद्धिक चिंताओं को बिना किसी अपवाद के अब तक अंग्रेजी के मुहावरे और आतंक के बीच व्यक्त किया जाता रहा है. जिस हिंदी को ब्रिटिश भारतविदों ने वर्नाकुलर भाषा के रूप में क्षेत्रीय अस्मिता प्रदान कर स्थापित किया,आजादी के बाद, जब उसके इस मिथक को तोड़कर राष्ट्रीय भाषा का जामा पहनाते हुए उसे भारतीय लोक-भावना के समानांतर विकसित करने की जरूरत थी, वह भारतीय बुद्धिजीवियों के बीच पहले की अपेक्षा अधिक गुलाम भाषा बनकर उभरी. यह अनायास नहीं है कि हिंदी-भाषी खुद अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए आज भी अंग्रेजी का ही सहारा लेते हैं.
इसी के साथ हिंदी के साथ एक और खतरनाक मिथक पैदा किया गया - अंग्रेजी और हिंदी की प्रतिस्पर्धा का; जैसे कि ये भाषाएँ न होकर एक दूसरे की दुश्मन हों. यह अनायास नहीं है कि भारतीय जन-अभिव्यक्ति से उसकी अपनी ज़बान छीनने के लिए अंग्रेजी आतंकित समाज ने संस्कृतनिष्ठ 'शुद्ध हिंदी' को संरक्षण देना शुरू किया. हिंदी का यह रूप भी एक तरह से तुष्टीकरण की प्रक्रिया थी, क्योंकि आम भारतीय के लिए यह भाषा भी उतनी ही दुरूह थी, जितनी कि अंग्रेजी. सदियों से भारतीयों द्वारा अर्जित ज्ञान-विज्ञान की थाती हमें अंग्रेजी द्वारा प्राप्त हुई थी; मगर यहाँ पर हमने वही गलती की जो संस्कृत के पंडितों ने हिन्दवी और हिंदी प्रदेश की दूसरी लोक-भाषाओँ के प्रति अपनाई. यही वजह थी कि हिंदी समाज की अपनी भाषा उसकी अभिव्यक्ति की भाषा कभी नहीं बन पाई.
हम लगातार आज भी वही गलती करते जा रहे हैं. मातृभाषाएँ ख़त्म हो रही हैं, उनका उपयोग हम अपनी जातीय भाषा के निर्माण और विन्यास के लिए नहीं कर पा रहे हैं. हिंदी की ताकत उसकी यही मातृभाषाएँ हैं. ध्यान देने की बात यह है कि इन भाषाओँ को आज के दिन उसी रूप में लौटाया नहीं जा सकता जिस रूप में उनका समाज वर्षों पहले उसे त्याग चुका है. उन्हें उस 'चमत्कार' के रूप में भी नहीं लौटाया जा सकता जिस रूप में 'नई कहानी' आन्दोलन के दौरान आंचलिक कथाकारों ने लौटाया था. भाषा का लौटना समाज के बगैर नहीं हो सकता.
यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि 'हिंदी समाज' से हमारा आशय क्या है? अधिकांश लोगों के दिमाग में हिंदी समाज का बिम्ब उन लोगों के रूप में उभरता है जो अंग्रेजी नहीं बोलता/बोल सकता, या आधुनिक दुनिया के चमत्कारों से वाकिफ नहीं है या उन्हें पसंद नहीं करता. क्या हिंदी समाज सिर्फ इतना ही है? क्या हिंदी समाज के बीच से वह शहरी मध्यवर्ग एकदम गायब हो चुका है जो भारतीय समाज की रीढ़ है?
जरूर शहरी मध्यवर्ग के बीच से उसकी मातृभाषाएं गायब होती जा रही हैं, मगर आज भी भारतीय समाज की जातीय भाषा हिंदी ही है. हमारी चिंता का सबब यही हिन्दी है, जो अशोक कुमार पाण्डेय के 'कश्मीरनामा' की हिंदी के रूप में सामने आई है. यह हिंदी फिक्शन की हिंदी भी नहीं है, जिसका आकर्षक प्रयोग अनेक प्रतिभाशाली कथाकारों ने विगत अनेक वर्षों में किया है, (हालाँकि वह भी हिंदी समाज की जातीय भाषा नहीं है).
'दखल प्रकाशन' का पुनर्जन्म इन्हीं अर्थों में एक ऐतिहासिक घटना है. मुझे खुद भी गर्व है कि इस प्रकाशन के आरंभिक चयन का एक हस्ताक्षर मैं भी हूँ. अंततः भारतीय हिंदी ही तो भारतीय समाज की जातीय अभिव्यक्ति होगी, जो दखल प्रकाशन की हिंदी किताबों जैसी ही होगी.