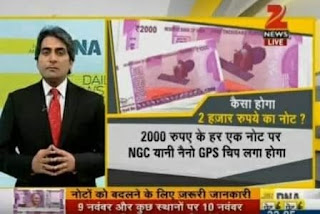||डी एस बी के गलियारों से||
( डिस्क्लेमर - इन क़िस्सों के सभी पात्र असली है. गोपनीयता की कोई गारंटी न देते हुए भी कहीं - कहीं नाम बदल दिये गये हैं.) देवसिंह बिष्ट डिग्री कॉलेज — ये नाम है उस डिग्री कॉलेज का जिसके कैम्पस में क़दम रखने के बाद जब भी कोई वहाँ से आख़िरकार बाहर गया होगा तो अपने साथ तमाम क़िस्से साथ ले गया होगा जो बढ़ती उम्र के साथ दिल और दिमाग की नसों में नत्थी हुए जाते हैं. स्कूल - कॉलेज के दिन वैसे भी सबसे ज़्यादा नौस्टैलजिया पैदा करते हैं.
यही कोई आठ - दस लड़कियों का एक ग्रुप था हमारा. स्कूल के दिनों में सख़्त अनुशासन से मिली नई - नई आज़ादी और कॉलेज में एडमिशन, वो भी नैनीताल जैसे पहाड़ी शहर में जिसकी हवाओं में एक ख़ास तरह की रूमानियत आज भी तैरती है. पर्यटकों के बोझ से दबे और बेतहाशा बेतरतीब तरीक़े से डेंजर ज़ोन में बनाई गई कई मंज़िला आधुनिक दिखने वाली इमारतों को ढोते हुए ये शहर आज किसी तरह बस हाँफते हुए जी रहा है. लेकिन ये अस्सी के दशक का नैनीताल था जहाँ की कुछ सड़कें मसलन अयारपाटा से होकर गुज़रती कॉलेज रोड दोपहर के समय इतनी वीरान होती थीं कि हम दो - तीन लड़कियाँ मिलकर भी उस वक़्त वहाँ से गुज़रने की हिम्मत नहीं करती थीं.
उन दिनों तक वहाँ बाइक या स्कूटरों की बाढ़ नहीं आई थी और जिन इने-गिने लोगों के पास ये दुपहिया वाहन थे उन्हें सारा शहर नाम से भले ही न जाने लेकिन वो फ़लाँ बाइक वाला लड़का या स्कूटर वाले अंकल जी मय उनकी बाइक या स्कूटर के रंग के साथ पहचाने जाते थे. कुछ के तो तीन डिजिट वाले नंबर भी कइयों को याद थे. ऐसे ही एक बंगाली डे अंकल की मुझे अब भी सिर्फ़ इसलिये याद है कि वे हमारे घर के पास रहते थे और उनके पास एक पीले रंग का स्कूटर था.
ख़ैर ... कॉलेज के फ़ॉर्म भरे गये और एडमिशन हो गये. स्कूली यूनीफॉर्म और बैग की जगह कंधों से लटकते पर्स और हाथों में इस अदा के साथ पकडी किताबों ने ले ली जो बाहर से देखने में अच्छी हों. किसी से ली गई पुरानी बेरंग कवर वाली किताबें कभी कभार ले जाने वाले और जतन से सँभाले गये पॉलीबैग के हवाले हुईं. मुश्किल से बचाए गये पैसों से बाक़ायदा शॉपिंग की गई.
बी. ए. की कक्षाओं का समय दस बजे का था. सभी के अलग अलग विषय तो थे लेकिन कॉलेज जाते हुए सबको साथ चाहिये था. जिनकी कक्षायें एक पीरियड बाद की होतीं वो भी अकेले इतनी दूर का रास्ता अकेले नापने के बजाय साथ जाने में ही भलाई समझतीं. रैगिंग का चलन तो नहीं था लेकिन लड़कियों के स्कूल से निकलने के बाद पहली बार को एड में पढ़ने का रोमांच भी था और भीतर एक अव्यक्त सा डर भी.
हम सब आसपास के मोहल्लों में रहा करते, तो पहले दिन से ही तय हो गया कि सब एक ख़ास जगह पर मिल कर वहीं से साथ - साथ कॉलेज जाया करेंगी . वो जगह थी बलरामपुर हाउस का गेट जहाँ सब ठीक समय पर पहुँच जाती. नई मिली आज़ादी को पंख भी लग गए लेकिन अभी उड़ना ठीक से नहीं सीखा था, ये भी एक वजह थी कि सब साथ मिलकर ही कॉलेज तक की तक़रीबन तीन किलोमीटर की दूरी पैदल नापते हुए साथ रहें. अकेले होने पर लड़कों के सामने पड़ते मन ही मन डर के मारे जान सूख जाया करती और हम चुपचाप उन्हें भरसक अनदेखा करने की कोशिश किया करते .
हमें अच्छी तरह पता था कि हमारे रास्ते में पड़ने वाले लड़कों के एकमात्र ब्रुकहिल हॉस्टल के लड़के ठीक तब पत्थर की आधी टूटी सी रेलिंग पर पैर झुलाते हुए लाइन से बैठ जाते जब हमारा वहाँ से निकलने का समय होता . वो ज़माना ही और था जब लड़के - लड़कियों के अपने -अपने ग्रुप हुआ करते थे और हम सब ऐसी व्यवस्था के आदी थे . ख़ैर ... जब हम इस बात से थोड़ा परेशान होने लगे कि हमें कॉलेज में नया समझकर हॉस्टल के लड़के कहीं हमें परेशान न करें तो उसका एक सीधा सा हल निकाला गया . वैसे तो हम दो - तीन लड़कियों का झुंड एक साथ चलता लेकिन जैसे ही स्विस होटल के बाद हॉस्टल का मोड़ आता हम आठ -दस लड़कियाँ पूरी सड़क घेरकर वहाँ से निकलतीं, सिर्फ़ ये जताने के लिए कि कम ना समझना, हम किसी से डरते - वरते नहीं . ये अलग बात है कि हॉस्टल पीछे छूटते ही हम जैसे कोई बड़ी चोटी फ़तह कर लेने की तरह अपनी इस ‘उपलब्धि’ पर ख़ूब हँसते . कुछ दिनों बाद हमारे इस ग्रुप का नामकरण हो गया था और अक्सर वहाँ से गुज़रते हुए हॉस्टल के लड़के एक दूसरे को आवाज़ लगाते हुए हमें सुनाते, “सेना आ गई बे सेना !”
कॉलेज पहुँचते तो वहाँ भी क्लासेज़ तक जाने के लिए एक ख़ूबसूरत मगर सँकरा सा लकड़ी के खंबों पर टिका टीन की छत वाला गलियारा था. आज भी है. वहाँ भी सहेलियों का साथ ही काम आता. अकेले - दुकेले होने पर तो सामने से आते लड़कों के झुंड साक्षात प्रेम चोपड़ा के भाई नज़र आते. इस तरह के लंबे लंबे गलियारे बरसात की मूसलाधार बारिश से बचने के लिये बनाए जाते थे जो इन पुरानी इमारतों का एक ज़रूरी हिस्सा बन गईं. फ़िल्मी स्टाइल में नायक - नायिका के आपस में टकराकर गिरती किताबें और फिर उन्हें उठाने के चक्कर में आँखें चार होने की ऐसे में पूरी संभावना थी लेकिन हमारी याददाश्त में ऐसा कभी हुआ नहीं.
शाम के चार बजे के आसपास क्लासेज़ ख़त्म होने पर सब वापस जाने के लिए निकलते. नैनीताल जैसी ख़ूबसूरत जगह, ऊपर से मौसम के हिसाब से रंग बदलती झील और रंग - बिरंगे हनीमून कपल्स. मुख्य बाज़ार से निकलते हुए इन जोड़ों की हम अक्सर आपस में मज़ाक़ बनाया करते. नये नवेले पति के एक हाथ में अक्सर कैमरा झूलता,आँखों पर सनग्लासेज, ज़्यादातर के बदन पर शादी के समय सिलाया गया थ्री पीस सूट और नवोढ़ा दुल्हन के पैरों में मेंहदी के बारीक डिज़ाइन के ऊपर चमकती पायल, हाथभर चूड़ियाँ और चटक रंग की साड़ी. कुछ पति तो अपनी पत्नियों के कँधे को दबाए ऐसे चलते जैसे इधर उसने हाथ हटाया और उधर वो भागी.
हमारी रास्ते भर की मस्ती ब्रुकहिल हॉस्टल के पास पहुँचते - पहुँचते काफ़ूर हो जाती. हालाँकि मुझे याद नहीं कि कभी कोई फब्तियाँ सुनने को मिलीं हों पर हमारी कोशिश रहती कि बस किसी तरह हॉस्टल झटपट पीछे छूट जाय. शाम के वक़्त लड़के हॉस्टल के ऐन नीचे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर झुंड बनाकर खड़े मिलते. कुछ उसके ठीक सामने के एक ढाबेनुमा चाय की दुकान में बैठे होते. तब हमारी हालत कुछ कुछ शेर की माँद से निकलने जैसी होती. दिनभर की थकान भी होती थी ऊपर से चढ़ाई का रास्ता. सुबह की तरह फु्र्र तो हुआ नहीं जाता था.
नैनीताल में बारिश आ पड़ने का कोई अंदाज़ा नहीं रहता. ऐसे ही एक दिन बारिश अचानक ही आ गई और सबके पास छाते भी नहीं, तो एक छाते में दो - दो मुंडियाँ घुसाए बस किसी तरह पूरा भीगने की शर्म से बचते बचाते हम वापस आ रहे थे. आज जहाँ अब हाईकोर्ट है वहाँ कभी सरकारी विभागों के दफ़्तर हुआ करते थे और वो आलीशान ऐतिहासिक ‘अंग्रेज़ों के ज़माने‘ की इमारत सेक्रेट्रियेट बिल्डिंग कहलाती थी. उस दिन उसकी चढ़ाई तक आते -आते बारिश बंद होकर धूप निकलने लगी. हम में से न जाने कौन कहीं से एक पंचांग उठा लाई थी और हम सब चाव से पंचांग की तिकड़मी गप्पों में इतने मशगूल थे कि किसी को छाते बंद करने का ख़याल ही नहीं रहा. किसी को ये होश नहीं रहा कि ब्रुकहिल आ गया है. जैसे ही हम हॉस्टल के सामने पहुँचे कि कई सारे लड़के ज़ोर से एक साथ चिल्लाए ..” धूप आ गई , धूप आ गई ....”
हमें तो जैसे साँप सूँघ गया. हड़बड़ी में छाते बंद किये. न रोते बना और हँसने का तो सवाल ही नहीं था. वहाँ से चाल में जो तेज़ी आयी तो उस मोड़ पर आकर थमी जहाँ से हॉस्टल दिखना बंद हो जाता है. वहाँ पहुँच कर इतनी देर से रोकी गई हमारी वो हँसी छूटी कि हमारे पेट दुखने लगे और आँखों से पानी बहने लगा.
तीस साल से भी ज़्यादा पुराना ये क़िस्सा याद आने पर आज भी उतना ही हँसाता है लेकिन अब वहाँ लड़कपन की नादानियाँ करने वाले दिल नहीं रहते जिनकी आँखों में गुपचुप किसी का इंतज़ार भी हो.
अब उस ब्रुकहिल हॉस्टल की कितनी ही यादों के ध्वंसाविशेषों पर एक बेनूर सी इमारत खड़ी है जो यूँ तो दिन भर लोगों की आवाजाही से गुलज़ार रहती है लेकिन जिसके अहाते में लगी रहने वाली भीड़ परेशानहाल लोगों से घिरे काले लबादे पहने लोगों से अपने अपने हिस्से का इंसाफ़ पाने की एक कभी न ख़त्म होने वाली प्रतीक्षा में चिंतित रहती है.
(चित्र - संगीता और तनुजा )