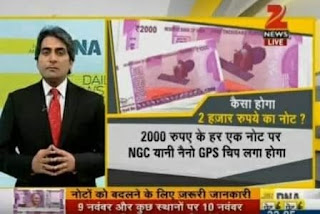||यह इंसानी फ़ितरत||
बचपन का वह दोस्त याद आता है जिसका परिवार किराए का घर बदलकर मज़बूरीवश श्मशान के ठीक सामने वाले नए घर में शिफ़्ट हुआ था। पहले दिन वह बेहद उदास था कि उसने एक मुर्दा जलते देखा था। दूसरे दिन उसने तीन शव अपने घर की खिड़की से राख होते देखे और थोड़ा उदास हुआ।
सप्ताह भर में वह इतना खुल गया कि घाट पर जाकर अंतिम क्रिया को देखने लगा। और महीने भर बाद वह बाकायदा तफ़सरा सुनाने लगा कि बीते दिन घाट पर जो शव जले उनमें कौन जवान था,कौन बूढ़ा....कितनी स्त्रियां थीं,कितने पुरुष ! समय और घटनाओं की आवृतियां धारणाओं की सलीब पर टंगे भय को यूं ही फ़ना करती हैं। चार महीने पहले विदेशों के कुछ ताबूत टी.वी.पर देखकर हमने अपने द्वार बंद कर दिए थे। अब हमारे श्मशान धधक रहे हैं और हम सड़कों पर टहल रहे हैं। लापरवाही कम, यह इंसानी फ़ितरत से प्रणोदित मामला ज़्यादा है।
वाइरस तो रहेगा, इसी के साथ जीना है। बढ़ते म्यूटेशन के साथ यह कम मारक होगा और फिर वैक्सीन भी तो आ रही है। ज़िंदगी रुकती थोड़े ही है। एक जो सैकड़ों साल पहले शव देखकर ठिठका था वह बाद में बुद्ध बना। उसके बाद तो कोई दूसरा बुद्ध बना नहीं...! डर का मरना भी डरावना होता है।