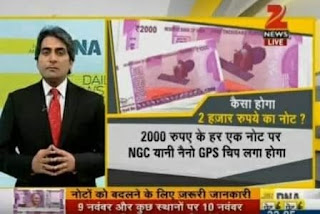वे आन्दोलनकारी नहीं बल्कि संस्कृतिकर्मी हैं
उत्तराखण्ड पहाड़ी राज्य में ''ढोल'' के बिना कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में ढोल व ढोली लुप्त प्रायः ही हो रहे है। इसके कई और कारण हो सकते है लेकिन ढोल का महत्व समझे बिना भी आगे बात करनी बेइमानी ही होगी। बताते चले कि इस पहाड़ी राज्य में बारह माह के बारह त्यौहार होते ही है। उदाहरणतः प्रत्येक माह की संक्रान्ती के दिन जो पूजा घरों व ''देव स्थलों'' में होती है वह ढोल की थाप पर ही आरम्भ होती है। मंदिरों में तो बाकायदा पण्डित जी जितने करतब पूजा-अर्चना बावत करता है उतने ही प्रकार के ताल मंदिर से कुछ गज दूर बैठा ''ढोली'' ढोल पर ध्वनी की उदत्त तरंगो से देता है।
यहां बता दें कि यही नहीं यह ढोली अपने ढोल को कंधो पर उठाकर बड़े उल्लास के साथ फिर गांव की प्रत्येक देहरी पर ढोल की थाप देता है और लोग तब अपने-अपने घरो में संक्रान्ती का पूजन आरम्भ करते है। तीज-त्यौहारों में भी यह ढोल जहां लोगों को गांव की चैपाल पर एकत्रित होने का आमन्त्रण देता है वहीं लोगों के मंनोरंजन करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। इसी तरह शादी-विवाह मंे भी ढोल व ढोली का अलग ही महत्व है। वे बारात के स्वागत से लेकर विदाई तक अपने ढोल के साथ पग-पग पर समारोह में उल्लास भरने में बेमिसाल उपस्थिति दर्ज करते हैं।
इसके अलावा जिस तरह वे शुभ अवसर पर ढोल की थाप को देने में मुस्तैद रहते हैं उसी तरह वे दुखः की घड़ी में भी उसी ढोल पर ऐसे स्वर-तालो की मार्मिक धुन प्रस्तुत करके दुखः के समय में गमगीन माहौल को भुलाने और भविष्य में कैसे अच्छा समय आये ऐसा वे शोक संदेश की 'ताल लहरी' का प्रवाह करते हैं। दरअसल यह कार्य तो ढोली समाज के लोग करते आये है और यह सचमुच में संस्कृति को भी बनाये हुए हैं।
संस्कृति के वनिस्पत वे अन्य सामाजिक प्रतिबद्धताओं पर भी खरा उतरतें हैं। देश-दुनियां में जितने भी जनआन्दोलन होते है उन आन्दोलनो की धार तेज करने में इनकी ढोल की थाप कमतर नहीं है। आगे ढोल और पीछे जुलूस ऐसा नजारा ही सम्पूर्ण आन्दोलन की शक्ल को प्रस्तुत करता आया है। जुलूस में सबसे आगे, स्वागत के लिए अगवानी, मेलो एवं नुमाईश में ढोल एवं ढोली की अनिवार्यता, तमाम सामाजिक गतिविधियो में जब ढोल की अनिवार्यता है तो फिर भी ढोली को असमानता का दंश झेलना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ढोली एक संस्कृतिकर्मी भी है तो वह आन्दोलनकारी भी है।
परन्तु इससे आगे वह एक खास प्रकार का शिल्पी ''दर्जी एवं नाई'' के रूप में रहा है। बहरहाल वर्तमान में ढोली के इनमें से एक हुनर को अन्य विरादरियों ने अपनाया हो लेकिन ढोली विरादरी को यह कार्य विरासत में ही मिला है। अब तो मेलो एवं नुमाईशो की शक्ले सरकारी बजट ने बदली दी है। उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ गांव कण्डाऊं के बचन दास जो ढोल सागर के मर्मज्ञ है वे कहते है कि ढोल सागर जैसे शास्त्र में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के अलग-अलग आयामो के ''श्लोक'' है जो मनुष्य को सौहार्दपूर्ण व्यवहार की दिशा अख्तियार करता है। कहते है कि जब से भौण्डा प्रवृत्ति के बैण्ड बाजो ने गांवों में दस्तक दी है तब से ढोल व ढोली का अस्तित्व ही संकट में है।
यही नहीं तब से वैमनस्य की भावना समाज में ज्यादा ही दिखाई दे रही है। वह यह भी मानते है जब ''ढोल'' के बिना कोई भी कार्य अधूरा है तो ढोली के साथ होता आया भेदभाव ही ''ढोल'' पर संकट का एक कारण है। टिहरी के ढोल वादक सोहन लाल बताता है कि कुछ दिन तो ढोल बजाने से राशन चल ही जाता है। आगे उन्होंने कहा कि यदि गांव की बारात में जाना होता है तो रात्री विश्राम के लिए गौशाला ही नसीब होती है। इसके अलावा उत्तरकाशी के सोहन दास, फूल दास, पिनाठिया दास, चमन दास चमोली के दिवानी राम, पिथौरागढ के भुवनराम देहरादून जौनसार क्षेत्र के सीन्नाराम जैसे ढोल वादक कहते हैं कि उन्हे प्रदर्शन के पश्चात ना तो एक तयशुदा मजदूरी मिलती है और ना ही उन्हे मान समान दिया जाता है। कहा कि जब तक ढोल नहीं बजेगा तब तक कोई भी कार्य आरम्भ ही नही होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक ढोल की आवश्यकता यहां के समाज को है। फिर भी ढोली समाज अछूता है।
सनद रहे कि देश भर में आयोजित व स्वस्फूर्त राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलनों में ढोल एक मुख्य कड़ी हैं इसकी गुंजायमान एक ही थाप लोगों को सोचने के लिए विवश कर देती है। लोक संस्कृति का संवाहक कहे जाने वाले ढोल की अन्य प्रतिस्पर्धा में भी एक खासा स्थान है।
हंसने की ताल, रोने की ताल, लड़ने की ताल, उत्तेजना की ताल, जोड़ने की ताल, नाचने की ताल, खेलने की ताल, आमन्त्राण की ताल, रूकने की ताल, बधाई संदेश की ताल, झकझोरने की ताल, देव अवतार की ताल पूजने व विसर्जन की ताल, सन्देश पहुंचाने की ताल, न जाने इस ढोल मंे हजारों ताल समाये है। इस सम्पूर्ण ढोल सागर की संगीत विद्या पर अध्ययन करने की आज की आवश्यकता है। हालांकि हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में ''ढ़ोल के संरक्षण'' बावत एक केन्द्र स्थापित हुआ था और कुछ कार्य भी हुए थे परन्तु वर्तमान में यह केन्द्र ढ़ोल को भुलाया बैठा और ''नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा'' की तर्ज पर कार्य करने लग गया है। कहा जा सकता है कि ढोल व ढोली पर एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। अब ढोल सिर्फ लोक संस्कृति कहे जाने तक ही सिमटता जा रहा है।
सामाजिक ताने-बाने में ढोली समाज अब हाशिये पर खड़ा हो चुका है। परन्तु ढोली समाज के लोग संस्कृति का बोेझ ढोने के लिए आज भी तैयार है।
ढोल और ढोल सागर
ढोल सागर भी एक महा ग्रन्थ है। उत्तराखण्ड मे इस ढोल की गाथा का इतिहास पांच हजार साल पुराना बताया जाता है। ढोल वादन के पारखी मंत्र तंत्र के अलावा जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी आयामो में ढोल की अनूगूंज का अनूठा प्रस्तुतिकरण करते है और इस ढोल के बिना उत्तराखण्ड में कोई भी शुभ-अशुभ कार्य आरम्भ नहीं होता है। सन्1926 से पहले ढोल विद्या मौखिक थी 1932 में पहली बार भवानी दत्त पर्वतीय ने ढोल सागर पुस्तिका प्रकाशित की। 60 के दशक में मोहन लाल बाबुलकर ने नद नंदनी पुस्तक लिखी जो आज भी अप्रकाशित है। 70 के दशक मे केशव अनुरागी,1976 मे अनूप चंदोला ने ढोल सागर पर किताब लिखी तो इन्ही दिनो प्रो.विजय कृष्ण ने शोध किया। 90 के दशक में आस्ट्रेलिया के न्यू इंग्लैण्ड विवि के प्रो.एन. रुवी ओल्टर ने डासिंग विद देवतास पुस्तक लिखी। कुलमिलाकर ढोल और ढोली पर पुस्तकें तो लिखी गयी परन्तु उस ढोली बिरादरी की आजीविका पर आज तक कोई सकारात्कम पहल सामने नहीं आई है।
आन्दोलनकारी जो अब तक घोषित न हो सके
-चन्द्र सिंह, सेनि॰ आईएएस॰
रामपुर तिराहा काण्ड के बारे में मुझे बारीकी से इसलिए जानकारी हुई थी,चूंकी मैं 02 अक्टूबर 1994 को स्वयं उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पद पर तैनात था। घटना की सूचना मिलने पर मैं भी रुड़की राजकीय चिकित्सालय मे जख्मी आन्दोलनकारियो को देखने गया था।
तत्काल जिलाधिकारी चमोली रहते हुए भी कई बार आन्दोलनकारियों को मिलने के लिऐ गैरसैण जाना पड़ा और आन्दोलन को उग्र होने से बचाने का प्रयास किया। सभी गांवो से जितने भी आन्दोलनकारियों की टोलियां मुख्य बाजारो एवं मुख्य स्थानो पर एकत्रित होती थी, की अगवाई ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा, तथा भेरी से स्थानीय बाजगी स्वतःस्पूर्त आन्दोलन के हिस्से के रूप में भाग लेते हुऐ मैने स्वयं देखा था। मेरी जानकारी मे सभी आन्दोलनकारी बाजगीयो सहित दिन भर भूखे रहते थे। यह कटु सत्य है कि आन्दोलन की अगवाई ढोल आदि लोक वाध्य यंत्रो की थाप से ही होती थी। जितनी अधिक ढोलो की संख्या उतना ही आन्दोलन में उत्साह बनता था। पता नहीं बाजगी समुदाय के लोग आन्दोलनकारियों की श्रेणी मे क्यों नहीं आऐ यह कौतुहल का विषय है। लिहाजा इसकी पुष्टी तत्कालीन जिलाधिकारियों से की जा सकती है। इस हेतु चिन्हित आन्दोलनकारी का कथन ही विश्वसनीय होगा।
सार्वजनिक स्वरूप के राष्ट्रीय महत्व के चारो धाम और राज्य स्तरीय व ग्राम स्तरीय जितने भी सार्वजनिक स्वरूप के मंदिर है,जिसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 25(2)(ख)में दी गयी है, के अनुरूप बाजगीयो के मान तथा सम्मान की व्यवस्था की जा सकती है। बदलते परिवेश ने इनके पारंगत व्यवसाय की मजदूरी वही पुराने ढर्रे पर आंकी जाती है। खेद इस बात का है कि श्रम विभाग एवं राजस्व विभाग ने भी बंधुवा मजदूर/सामुहिक बंधुवा मजदूरो के साथ-साथ बाजगी समुदाय की स्थिति की न तो समीक्षा की और न ही वर्तमान स्थिति को जानने का प्रयास किया गया। उत्तराखड के अधिकांश हिस्सो में आज भी यह प्रथा मौजूद है कि मुर्दे की अर्थी के आगे-आगे ढोल बजाते हुऐ बाजगी को मुर्दाघाट तक जाना पड़ता है।