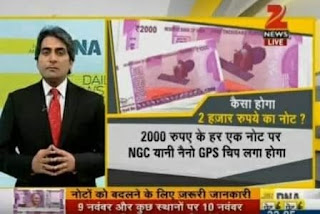||झाड़ू मार दिया, आज रात को तुझे बाघ ले जाएगा||

आज बात- " झाऊण (झाड़ू) और बाबिल" की। ये वही "झाऊण" था जिससे मारने पर बाघ ले जाता था। यह करामाती झाऊण, बाबिल से ही बनता था। "बाबिल" मतलब एक ऐसी घास जिसका पहाड़ी जीवन के साथ जीवन-मरण का संबंध था। यह गाय-भैंस से लेकर मनुष्य तक की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा था। पहाड़ की आत्मनिर्भरता का कुछ बोझ बाबिल के हिस्से भी था।
भ्योव (जंगल) में बाबिल बहुत होता था। बाबिल की घास बहुत पैनी होती थी। इतनी पैनी की आपका हाथ भी काट सकती थी । इसके बड़े-बड़े 'बोट'' (गुच्छे) होते थे। 'जंगों' (जंगल) में 'घा' (घास) बांधने से लेकर घर में बाड़ बांधने तक के लिए इसका ही उपयोग किया जाता था। ईजा ऐसे किसी भी काम के लिए कहती थीं- "बाबिलेल बांध दे उकें"(उसको बाबिल से बांध दे)। एक तरह से हरफनमौला घास थी।
ईजा जब भी घास लेने जाती तो उन्हें जहाँ भी बाबिल दिखाई देता तो उसे अलग से काट कर रख लेती थीं। कभी-कभी तो हमको कहती थीं -"ऊ के भोल बाबिलक बोट है रहो, काट ढैय् च्यला" ( वो कितनी अच्छी बाबिल की घास हो रखी है, बेटा काट उसे )। हम उसे आराम -आराम से काटते थे। हरी बाबिल की घास को तो काट सकते थे लेकिन सूखे को काटना बड़ा मुश्किल होता था। मजबूत सी घास होती थी।
ईजा घास के 'पु' (घास का थोड़ा ढेर) बांधने के लिए भी कभी-कभी बाबिल घास का इस्तेमाल करती थीं। अगर हम सूखी या कच्ची लकड़ी के लिए "ज्योड" (रस्सी) ले जाना भूल जाते या कहीं छूट जाती तो ईजा 'चट' (तुरंत) से बाबिल काटती और उसको रस्सी की तरह बनाकर लकड़ी बांध देती थीं। कहती थीं-"भलि लीजिए बाबिल ले बांध रहो, ख़सिक जाल"( अच्छे से ले जाना, बाबिल से बांध रखा है, खिसक जाएगा)। हम लकड़ी सर पर लेकर ईजा के आगे माठु-माठु (धीरे-धीरे) चल देते थे।
ईजा हरा बाबिल अक्सर "छन के पख' (गाय-भैंस जहां बांधते हैं, उसकी छत) में सूखने के लिए रख देती थीं। सूख जाने के बाद उसे "छनक गोठ" संभाल कर रखती थीं। बाबिल के लिए 'छनपन' ही नियत जगह होती थी। उसे घर नहीं ले जाते थे। घर तभी लाते थे जब झाड़ू बनाना हो।
बाबिल की घास से "झाऊण" (झाड़ू) बनता था। यह एक असाधारण कला थी। हर कोई झाऊण नहीं बना सकता था। ईजा रात से बाबिल को जहाँ पानी की गगरी रखी रहती थी वहीं नीचे या बाल्टी में भिगो देती थीं। उसके बाद सुबह धूप में "बुबू" (दादा) 'झाऊण' बनाते थे। झाऊण बनाने का नियम था। उसे दिन ढलने के बाद और सुबह-सुबह नहीं बना सकते थे। अगर कोई सुबह-सुबह बनाने बैठ जाता था तो गुस्से वाले भाव में कहते थे- "राति-राति पर बाबिल लिबे बैठ गो" (सुबह-सुबह बाबिल लेकर बैठ गया है)। कुछ इसे अपशगुन भी मानते थे।
हमारे घर में 'बुबू' (दादा) ही झाऊण बनाते थे। जब बुबू नहीं रहे तो कभी "मकोट" (ननिहाल) के तो कभी गाँव के एक बुबू बना देते थे। एक बार में बुबू छोटे-बड़े तीन-चार झाऊण बनाते थे। उनमें हम बच्चों के लिए भी एक-एक होता था। कहते थे-"नतिया य तिहें बने रो" (नाती ये तेरे लिए बना रखा है)। हम अपना झाऊण देखकर बड़ा खुश हो जाते थे और तुरंत उसे गोठ या भतेर संभाल देते थे।
झाऊण बनाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बराबर करने के लिए 'दिहे' (देहरी) में रख कर काटा जाता था। काटने से पहले झाऊण में और दिहे में "झुंगर" (एक अनाज) के कुछ दाने रखे जाते थे। बिना उन्हें रखे नहीं काटा जाता था। हमने बुबू को 'दिहे' के अलावा और कहीं काटते हुए भी नहीं देखा था।आज भी यही चल रहा है।
यह झाऊण सिर्फ "गोठ-भतेर" (घर के अंदर और नीचे) में झाड़ू लगाने के काम ही नहीं आता था बल्कि मंत्र विद्या में भी इसका उपयोग होता था। जब भी किसी की पीठ में "हुक"(पीठ में ऊपर से लेकर नीचे को अचानक दर्द होना) पड़ती थी तो उसे 'दिहे' में बिठाकर झाऊण से ही झाड़ा जाता था। बाद के दिनों में तो मैं भी इस 'हुक' झाड़ने के काम में पारंगत हो गया था। ईजा कई बार कहती थीं- "च्यला ऊ पारेकि आमक हुक झाड़ी हा" (बेटा जरा सामने वाली दादी की हुक झाड़ आ)। हो.. होई... कहकर, मैं दिन छिपने के बाद निकल पड़ता था। वहाँ फिर यही झाड़ू काम आता था।
झाऊण को लेकर एक और किस्सा भी थी। कहते थे अगर किसी को 'झाऊण' से मार दो तो उसे बाघ ले जाता है। ईजा कहती थीं- "झाऊणेल नि मार उकें बाग लि जाल" (उसको झाड़ू से मत मार, बाघ ले जाएगा)। हम कई बार जानबूझकर एक-दूसरे को झाऊण से मारते थे और कहते थे- "ले, आज रात हैं तिकें बाग लिजाल" (मार दिया आज रात को तुझे बाघ ले जाएगा)...
अब इस झाड़ू का कम ही प्रयोग होता है। फिर भी हमारे घर और गांव में तो अभी ये प्रचलन में है। ईजा कहती हैं- "मैंकें त येकि सार ऐंछि" ( मुझे तो यही ठीक लगता है)। ईजा अब भी इसी झाड़ू को गाँव के एक बुबू से बनवा लेती हैं। उनकी दुनिया में "झाऊण" का इतिहास अभी बदला नहीं है